भारत की आत्मा केवल भूगोल में नहीं बसती — वह उसकी संस्कृति, सामाजिक व्यवस्था और सहस्राब्दियों से चली आ रही उस चेतना में निहित है, जिसने विभिन्नता को विरोध नहीं, बल्कि संवाद और समरसता का माध्यम बनाया। यह वह भूमि रही है जहाँ सामाजिक विषमताओं का समाधान प्रतिशोध नहीं, धर्म और मर्यादा के आलोक में खोजा गया। परंतु आज एक नया संकट खड़ा हो रहा है — ऐसा संकट जो न्याय के नाम पर असंतुलन, समानता के नाम पर घृणा और संवेदनशीलता के नाम पर वैमनस्य को संस्थागत रूप देने का प्रयास कर रहा है।
इस संकट की नवीनतम अभिव्यक्ति है — ‘रोहित वेमुला (उत्पीड़न निवारण और शिक्षा में सम्मान का अधिकार) विधेयक’, जिसे कर्नाटक की कांग्रेस सरकार आगामी विधानसभा सत्र में प्रस्तुत करने की योजना बना रही है। यह कोई साधारण कानूनी प्रस्ताव नहीं है — यह भारत में कल्चरल मार्क्सवाद के वैचारिक प्रभाव का एक स्पष्ट द्योतक है। यह विधेयक न तो केवल शैक्षणिक सुधार का उपक्रम है, और न ही केवल सामाजिक न्याय का यत्न — अपितु यह उस दीर्घकालिक वैचारिक युद्ध का अगला चरण है, जिसमें भारत की एकता, शिक्षा और आत्मबोध को एक नये प्रकार की "संरचनात्मक वैमनस्यता" से प्रदूषित करने की योजना है।
यह प्रस्ताव कहता है कि यदि कोई अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग अथवा अल्पसंख्यक समुदाय का छात्र यह शिकायत करता है कि उसके साथ संस्थान में भेदभाव हुआ है, तो संस्थान के अधिकारी के विरुद्ध संज्ञेय एवं गैर-जमानती अपराध के अंतर्गत कार्यवाही होगी। दोष सिद्ध होने पर कारावास, आर्थिक दंड, वित्तीय सहायता की समाप्ति, और पीड़ित छात्र को प्रतिकर की अनिवार्यता इस प्रस्ताव के कुछ प्रमुख प्रावधान हैं।
यहाँ प्रश्न उठता है — क्या वर्तमान भारत में ऐसे उत्पीड़न के विरुद्ध विधिक व्यवस्था पहले से मौजूद नहीं है? क्या अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम (SC/ST Atrocities Act), शिक्षा में आरक्षण, छात्रवृत्तियाँ, विशेष योजनाएँ, अल्पसंख्यक आयोग — ये सब असमर्थ रहे हैं? यदि नहीं, तो यह नया विधेयक क्यों?
इसका उत्तर हमें केवल भारत के भीतर नहीं, अपितु अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका की वैचारिक प्रयोगशालाओं में खोजना होगा — वहाँ जहाँ कल्चरल मार्क्सवाद नामक वैचारिक विष को 'न्याय' और 'समानता' की पोशाक पहनाकर समाजों को भीतर से तोड़ने का क्रम आरंभ हुआ।
20वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में अमेरिका के कुछ विश्वविद्यालयों, विशेषतः हार्वर्ड लॉ स्कूल, बर्कले और येल जैसे संस्थानों में एक नया विचार पनपने लगा। यह विचार था — क्रिटिकल रेस थ्योरी (CRT)। प्रारम्भ में यह एक विधिशास्त्रीय विमर्श के रूप में सामने आया, परंतु शीघ्र ही यह अमेरिका के राजनीतिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को गहराई से प्रभावित करने लगा।
CRT का मूल कथन यह था कि — अमेरिका की समस्त संस्थाएँ — न्यायपालिका, प्रशासन, शिक्षा, और यहाँ तक कि भाषा और विज्ञान भी — एक नस्लीय संरचना पर आधारित हैं, जिसे "श्वेत वर्चस्व (White Supremacy)" के बनाए रखने के लिए निर्मित किया गया है। अतः, श्वेत समाज का प्रत्येक व्यक्ति — चाहे वह व्यक्तिगत रूप से भेदभाव करे या न करे — इस संरचना का लाभार्थी है, और इस प्रकार वह संरचनात्मक रूप से 'रेसिस्ट' है।
CRT ने क्या किया?
इस विचारधारा ने समाज में एक नया विभाजन पैदा किया:
1. श्वेत = जन्मना शोषक
2. अश्वेत = जन्मना पीड़ित
अब व्यक्ति के नैतिक आचरण, संवेदनशीलता, परिश्रम या मानवीय दृष्टिकोण का कोई मूल्य नहीं रह गया। केवल उसकी नस्ल ही यह तय करती थी कि वह अन्यायी है या अन्याय का शिकार।
विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में CRT के आधार पर "diversity training", "whiteness studies", "anti-racism workshops" चलाए गए, जहाँ बच्चों को यह सिखाया गया कि वे श्वेत हैं तो उनके पूर्वजों ने गुलामी और अन्याय किया है, और इसलिए उन्हें इस ऐतिहासिक अपराध का "पछतावा" होना चाहिए। अश्वेत छात्रों को यह सिखाया गया कि उनकी असफलता या पिछड़ापन उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं, अपितु व्यवस्था द्वारा सुनियोजित उत्पीड़न का परिणाम है।
इसका प्रभाव यह हुआ कि अमेरिका में:
शिक्षा पर से विश्वास डगमगाया, क्योंकि विद्यार्थियों को परिश्रम से नहीं, पीड़ित-तत्व से मूल्यांकन मिल रहा था।
समाज में अपराधबोध और घृणा की दो धाराएँ बन गईं — एक आत्मग्लानि से ग्रस्त, दूसरी प्रतिशोध से प्रेरित।
लोकतांत्रिक संवाद समाप्त हो गया, क्योंकि हर असहमति को नस्लवाद घोषित कर दिया गया।
पारिवारिक और धार्मिक संस्थाओं पर हमला हुआ, क्योंकि उन्हें ‘श्वेत पितृसत्ता’ की संरचना कहा गया।
आज अमेरिका में यह स्थिति है कि:
विश्वविद्यालयों में प्रवेश केवल योग्यता से नहीं, नस्लीय कोटे से होता है।
श्वेत छात्र डरते हैं कि उनकी किसी सामान्य टिप्पणी को भी नस्लभेदी घोषित कर दिया जाएगा।
शिक्षकों और कर्मचारियों को अनिवार्य ‘anti-racism confession programs’ से गुजरना पड़ता है।
यह समाज को न्यायसंगत बनाने का प्रयास नहीं था — यह एक नई वर्ग-संघर्ष आधारित वैचारिक क्रांति थी, जिसमें 'शोषण और प्रतिरोध' की साम्यवादी परंपरा को नस्लीय परिप्रेक्ष्य में ढालकर प्रस्तुत किया गया।
भारत में इसका प्रतिबिंब — जाति की आड़ में ‘क्रिटिकल कास्ट थ्योरी’
आज वही विचारधारा भारत में 'जाति' के नाम पर उतारी जा रही है। अंतर बस इतना है कि यहाँ नस्ल की जगह जाति ने ले ली है:
यहाँ 'श्वेत' की जगह 'सवर्ण' है,
'अश्वेत' की जगह 'एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक' हैं,
और 'White Guilt' की जगह 'Upper Caste Guilt' का विमर्श।
‘रोहित वेमुला विधेयक’ उसी CRT के जातिगत संस्करण की प्रस्तावना है — जहाँ संस्थान में एक सामान्य छात्र या शिक्षक को, केवल जाति के आधार पर, ‘संरचनात्मक अपराधी’ मानकर कानूनी दंड का पात्र बना दिया जाएगा। यह वही रणनीति है, जिसने अमेरिका को गहरे सामाजिक तनाव, परस्पर संशय, और राष्ट्रविरोधी प्रवृत्तियों में धकेल दिया — और अब भारत को उसी मार्ग पर ले जा रहा है।
राहुल गांधी द्वारा कर्नाटक के मुख्यमंत्री को लिखा गया पत्र इस बात का प्रमाण है कि यह केवल राज्य स्तर का प्रस्ताव नहीं, अपितु एक राष्ट्रव्यापी वैचारिक प्रयोग की तैयारी है। कांग्रेस वर्षों से यह नीति अपनाती रही है — 2011 का "सांप्रदायिक और लक्षित हिंसा निवारण विधेयक" इसका उदाहरण है, जिसमें हर दंगे के लिए केवल बहुसंख्यक हिन्दू समाज को दोषी मानने की विधिक व्यवस्था प्रस्तावित थी।
अब उसी धारा में जातीय संघर्ष को शिक्षण संस्थानों में स्थापित करने का प्रयास हो रहा है — जहाँ छात्र पढ़ाई नहीं, उत्पीड़न की राजनीति में शिक्षित होंगे; जहाँ शिक्षक शिक्षा नहीं, अपराधबोध से ग्रस्त प्रशासन बनाएँगे।
यह कोई नीतिगत त्रुटि नहीं, यह पूर्वनियोजित वैचारिक योजना है — जिसका उद्देश्य है भारत में वैचारिक गृहयुद्ध की भूमि तैयार करना, जहाँ जाति न्याय का नहीं, सत्ता संघर्ष का हथियार बने।
कांग्रेस यह भलीभाँति जानती है कि सवर्ण समाज, सामान्य वर्ग, हिन्दू शिक्षक या छात्र राजनीतिक रूप से संगठित नहीं हैं — उन्हें बार-बार अपराधबोध और पितृ-संस्कार के नाम पर चुप कराया जा सकता है। और उसी मौन का लाभ उठाकर 'न्याय के नाम पर प्रतिशोध' की राजनीति को वैधानिक रूप दिया जा सकता है।
यह विधेयक भले ही आज केवल एक 'प्रस्ताव' हो, परन्तु इसकी आत्मा गहरी है। यह भारत के शैक्षणिक परिसर में संरचनात्मक संघर्ष का बीज रोपता है — और वह संघर्ष पीड़ित को उन्नत करने का नहीं, अपितु समाज को खंडित करने का मार्ग प्रशस्त करेगा।
यह समय केवल प्रतिक्रिया का नहीं, प्रत्युत्तर का है। यदि हिन्दू समाज, सामान्य वर्ग, और राष्ट्रप्रेमी नागरिक इस वैचारिक षड्यंत्र को नहीं पहचानते — तो आने वाला युग शिक्षा में न्याय नहीं, अधिकारों का अराजक युद्ध लेकर आएगा।
भारत में न्याय की परंपरा संतुलन से चलती आई है — ना तो प्रतिशोध से, ना ही अपराधबोध से।
रोहित वेमुला विधेयक को एक तात्कालिक राजनीतिक प्रयोग न मानें। इसे पहचानिए — यह कल्चरल मार्क्सवाद की वही छाया है, जिसने अमेरिका को नस्लवाद में, यूरोप को धार्मिक विघटन में और अफ्रीका को जातीय गृहयुद्ध में झोंक दिया।
यदि यह विचार भारत में विधायी रूप ले लेता है, तो उसके बाद संघर्ष केवल वर्गों के बीच नहीं, पीढ़ियों के बीच भी होगा।
और तब यह प्रश्न उठेगा — क्या हमने अपनी संस्कृति की चेतना को केवल राजनीतिक लाभ के लिए बलि चढ़ा दिया?
✍️दीपक कुमार द्विवेदी
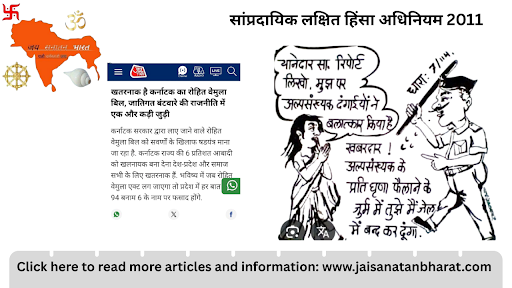
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें